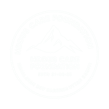उत्तराखंड, जिसे ‘देवभूमि’ कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक धरोहर, और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इन पहाड़ी गढ़ियों में कुछ ऐसी वीरानियाँ भी छिपी हैं—भूतिया गाँव, जिनमें जीवन की चहल-पहल समाप्त हो चुकी है। HDDUS CARE FOUNDATION के ब्लॉग लेखक मनोज गड़िया की मुलायम कलम और तथ्यात्मक दृष्टि इन वीरान गलियों को पुनर्जनन की रौशनी से फिर से जगाने का प्रयास करती है।
HDDUS CARE FOUNDATION के इस ब्लॉग में, हिंदी लेखक मनोज गड़िया की संवेदनशील लेखनी के माध्यम से हम उत्तराखंड के भूतिया गाँवों की विस्तृत कहानी, उनके पीछे के कारण, और इन गाँवों को पुनर्जनन करने की हमारी पहल पर प्रकाश डालेंगे।

भूतिया गाँव: एक दर्दनाक हकीकत
‘भूतिया गाँव’ शब्द सुनते ही मन में डरावनी कहानियों या अलौकिक घटनाओं का ख्याल आ सकता है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में यह शब्द पलायन की त्रासदी को दर्शाता है। ये वे गाँव हैं, जहाँ की आबादी पूरी तरह या लगभग पूरी तरह से शहरों की ओर पलायन कर चुकी है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में 1726 गाँव पूरी तरह निर्जन हो चुके हैं, और 398 ऐसे गाँव हैं, जहाँ लोग पलायन कर स्थायी रूप से अन्यत्र बस गए हैं। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में ये गाँव विशेष रूप से देखे जा सकते हैं।
मनोज गड़िया , जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, ने इन गाँवों की स्थिति को अपनी एक कहानी में इस तरह व्यक्त किया है: “ये गाँव भूतों के नहीं, बल्कि हमारी उपेक्षा और गलत नीतियों के शिकार हैं। इन खाली घरों में अभी भी उन परिवारों की यादें गूँजती हैं, जो कभी यहाँ बसे थे।”
भूतिया गाँव बनने के कारण
उत्तराखंड के गाँवों के वीरान होने के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय कारण हैं। आइए, इन पर विस्तार से नजर डालें:
- बड़े पैमाने पर पलायन
पलायन उत्तराखंड के भूतिया गाँवों का सबसे बड़ा कारण है। रोजगार के अवसरों, बेहतर शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण गाँवों के युवा शहरों जैसे देहरादून, दिल्ली, या अन्य मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। 2008 से 2018 के बीच, लगभग 5,02,717 लोगों ने उत्तराखंड से पलायन किया, और 2018 से 2022 के बीच यह संख्या 3,35,841 तक पहुँच गई, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह का पलायन शामिल है। मनोज गड़िया ने अपने एक लेख में लिखा, “पहाड़ का युवा जब शहर की चमक-दमक की ओर जाता है, तो वह अपने गाँव की आत्मा को पीछे छोड़ जाता है।”
- प्राकृतिक आपदाएँ
उत्तराखंड एक भूकंपीय क्षेत्र है, जहाँ भूस्खलन, बाढ़, और ग्लेशियर फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आम हैं। जलवायु परिवर्तन ने इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को और बढ़ा दिया है। कई गाँव इन आपदाओं के कारण रहने योग्य नहीं रहे, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर गए।
- बुनियादी सुविधाओं की कमी
पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पलायन का एक प्रमुख कारण है। अधिकांश गाँवों में स्कूल और अस्पताल या तो हैं ही नहीं, या बहुत दूर हैं। गारिया ने इस मुद्दे पर लिखा, “जब एक माँ को अपने बच्चे के इलाज के लिए 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, तो वह गाँव में रहने का साहस कैसे जुटाएगी?”
- कृषि की असफलता
उत्तराखंड के गाँवों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन खेती अब लाभकारी नहीं रही। बंजर होती जमीन, जंगली जानवरों का खतरा, और सामुदायिक समर्थन की कमी ने किसानों को मजबूर कर दिया है कि वे खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करें।
- सामाजिक और सांस्कृतिक टूटन
पलायन के कारण गाँवों में सामुदायिक जीवन लगभग खत्म हो चुका है। पहले गाँवों में सामूहिक उत्सव, जागर, और मेले सामाजिक एकता का प्रतीक थे, लेकिन अब ये परंपराएँ भी लुप्त हो रही हैं। गारिया ने अपनी एक कविता में इस दर्द को व्यक्त किया है:
“खाली गाँव, खामोश रास्ते,
कहाँ गए वो मेले, वो हँसी के बस्ते?”
कुछ चर्चित भूतिया गाँव
- मटियाल गाँव (पिथौरागढ़)
मटियाल गाँव कभी पलायन के कारण पूरी तरह वीरान हो गया था, लेकिन 2020 में दो युवा, विक्रम मेहता और दिनेश सिंह, ने गाँव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जनन करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्थानीय खेती और बागवानी को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीन अन्य परिवार भी वापस लौट आए। गारिया ने इस प्रयास की सराहना करते हुए लिखा, “मटियाल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो वीरान गाँव भी फिर से गुलज़ार हो सकते हैं।”
- उमरेठ गाँव (गढ़वाल)
उमरेठ गाँव की 82 वर्षीय बुंदी देवी इस गाँव की आखिरी निवासी हैं। 12 साल की उम्र में शादी, 30 की उम्र में विधवा होने, और बेटों से अलगाव के बाद, वह अकेली इस गाँव में रहती हैं। उनकी कहानी पलायन की त्रासदी को जीवंत रूप से दर्शाती है।
- सेमला गाँव
सेमला गाँव की कहानी को पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र “एक था गाँव” में चित्रित किया गया है, जो यहाँ की महिलाओं की संघर्षशीलता और साहस को दर्शाता है। यह गाँव पलायन के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है।
- सौर गाँव (टिहरी)
सौर गाँव, जो कभी 2000 से अधिक लोगों का घर था, पलायन के कारण खाली हो गया था। लेकिन ‘Wise Wall Project’ और सामुदायिक पर्यटन परियोजनाओं ने इसे फिर से जीवंत करने में मदद की है।
HDDUS CARE FOUNDATION की पहल
HDDUS CARE FOUNDATION उत्तराखंड के भूतिया गाँवों को पुनर्जनन करने और पलायन को रोकने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। हमारी प्रमुख पहल में शामिल हैं:
- स्थानीय रोजगार सृजन
हम गाँवों में हस्तशिल्प, जैविक खेती, और पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमारी ‘पहाड़ी हस्तशिल्प’ परियोजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ
हम गाँवों में प्राथमिक स्कूल, मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक, और डिजिटल शिक्षा केंद्र स्थापित कर रहे हैं, ताकि परिवारों को गाँव छोड़ने की जरूरत न पड़े।
- पर्यावरण संरक्षण
जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हम वृक्षारोपण, जल संरक्षण, और भूस्खलन रोकथाम परियोजनाएँ चला रहे हैं। हमारा मानना है कि पर्यावरणीय स्थिरता गाँवों के पुनर्जनन का आधार है।
- सांस्कृतिक पुनर्जन
उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम जागर, लोक नृत्य, और पारंपरिक उत्सवों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी ‘लोक संस्कृति संरक्षण’ कार्यशालाएँ युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने का काम कर रही हैं।
मनोज गड़िया ने हमारी इन पहलों की सराहना करते हुए लिखा, “HDDUS CARE FOUNDATION केवल गाँवों को बचा नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को फिर से जगा रहा है। यह एक ऐसी मशाल है, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है।”
भविष्य के लिए रणनीति
उत्तराखंड के भूतिया गाँवों को बचाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख सुझाव:
बुनियादी ढांचे का विकास: गाँवों में सड़क, बिजली, और इंटरनेट जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित करना।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना: पर्यटन, हस्तशिल्प, और जैविक खेती को बढ़ावा देकर गाँवों में रोजगार सृजन।
शिक्षा और स्वास्थ्य: प्रत्येक गाँव में कम से कम एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना।
सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय समुदायों को नीति निर्माण में शामिल करना, ताकि उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए।
युवाओं को प्रेरित करना: डिजिटल शिक्षा और स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से युवाओं को गाँवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष
उत्तराखंड के भूतिया गाँव केवल खाली घरों और वीरान खेतों की कहानी नहीं हैं; ये हमारी सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय नीतियों की असफलता का प्रतीक हैं। लेकिन इन गाँवों में अभी भी जीवन की संभावना बाकी है। HDDUS CARE FOUNDATION, लेखक मनोज गड़िया की प्रेरणादायक लेखनी और विचारों के साथ, इन गाँवों को फिर से बसाने, उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने, और पलायन की इस त्रासदी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।